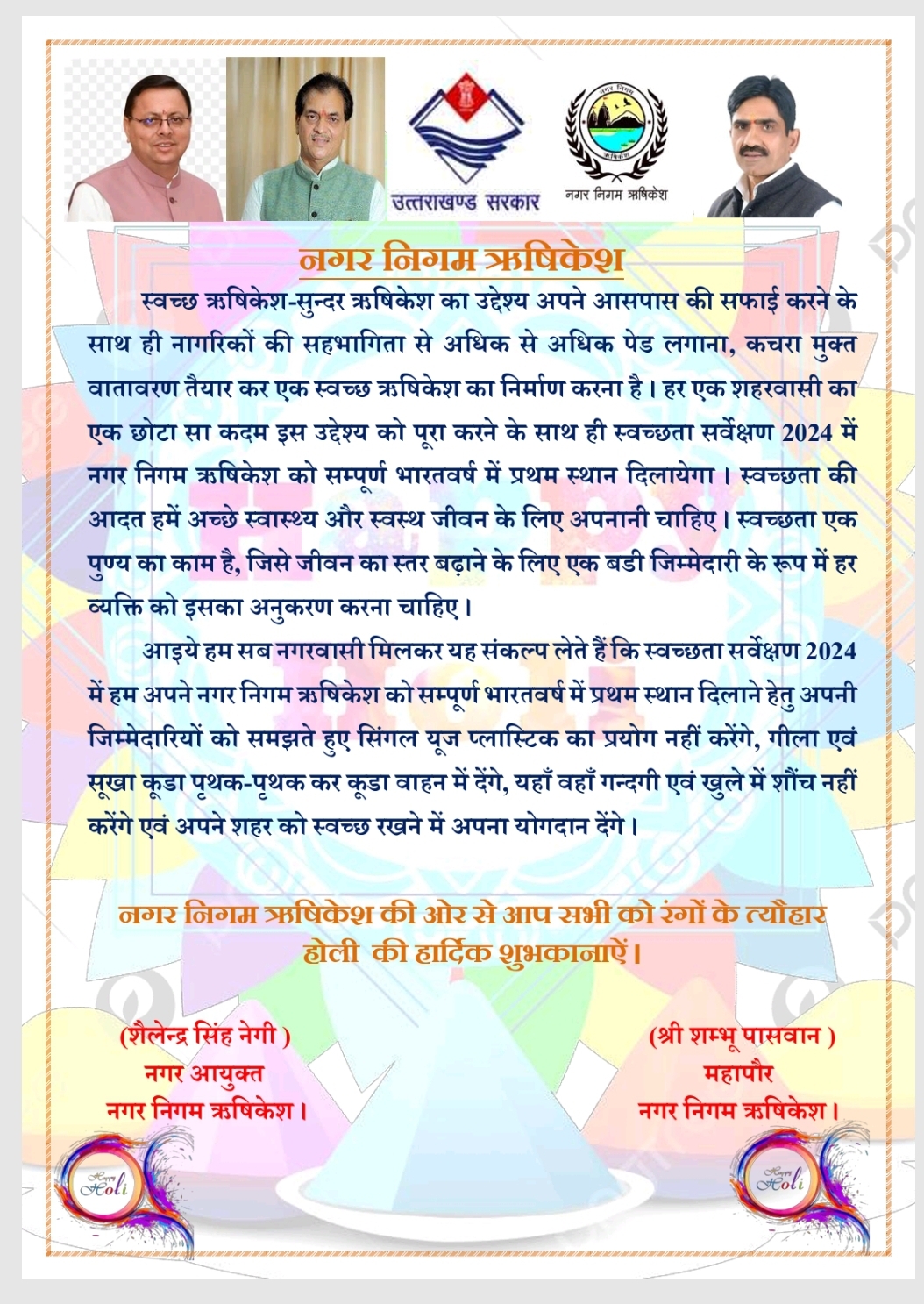“गांव की दीवारों पर उगते सवाल: उत्तराखंड का खोता आत्मबोध और पुनरावलोकन की पुकार



समाजसेवी चिंतक:रतन सिंह असवाल की कलम से
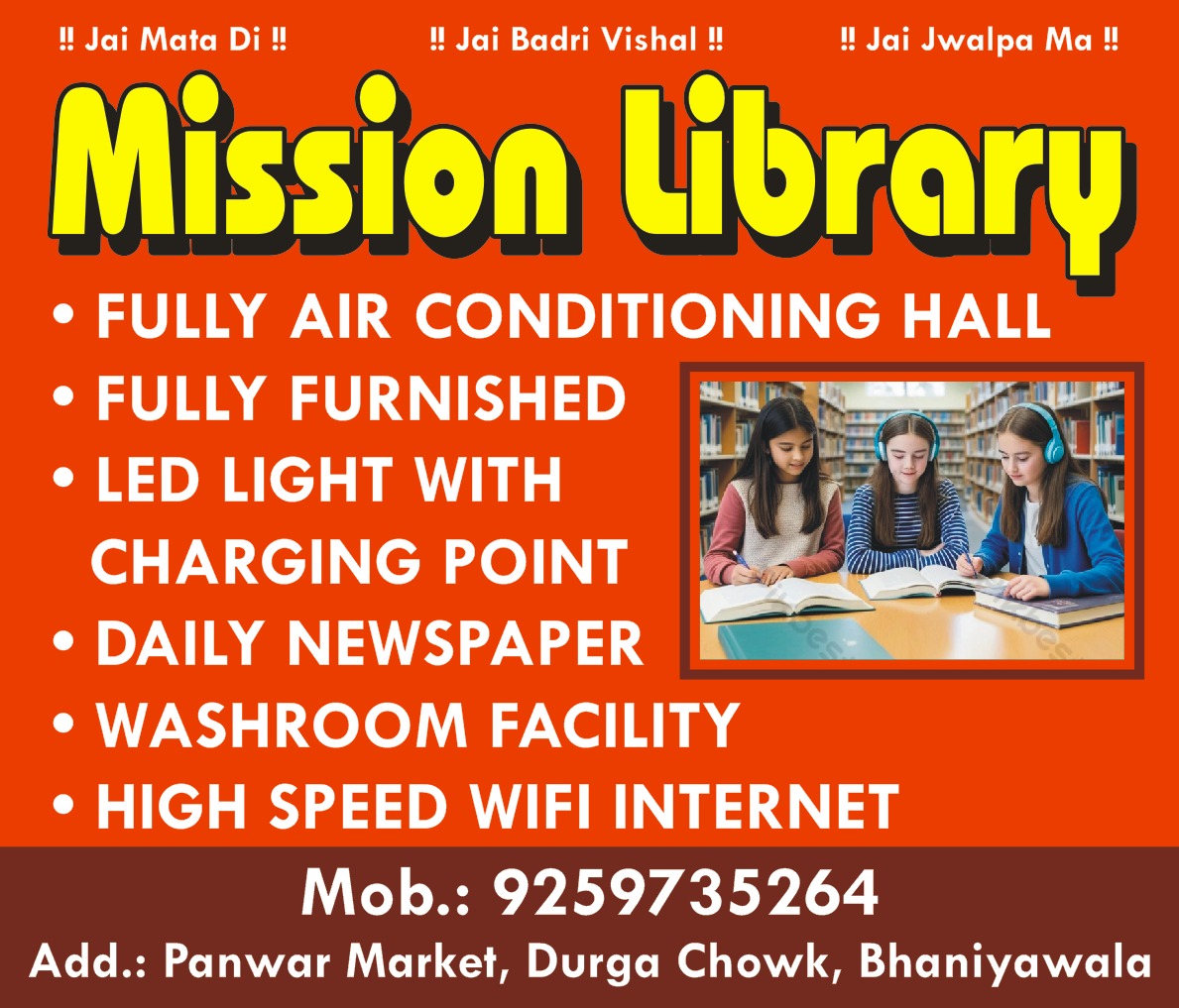

उत्तराखंड राज्य को बने पच्चीस वर्ष पूरे हो चुके हैं। यह राज्य केवल 13 जिलों की प्रशासनिक व्यवस्था भर नहीं था, बल्कि यह आंदोलन एक गहरी चेतना का स्वरूप था! जहां गांव, जंगल और जनजीवन की रक्षा की आकांक्षा थी।

लेकिन आज जब हम आत्मचिंतन करें, तो पाते हैं कि जिन गांवों को इस राज्य की आत्मा कहा गया, वे अब उपेक्षा और पलायन की पीड़ा के केंद्र बन चुके हैं।
वर्ष 2018 की “पलायन आयोग” की रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड के 6,338 गांवों में से 734 गांव पूरी तरह से “गोस्ट्र गांव” यानी वीरान हो चुके हैं। 3,946 गांव आंशिक रूप से खाली हो चुके हैं। अलग बात है कि आयोग खुद पलायन कर गया । रिपोर्ट के अनुसार हर दिन औसतन 100 से अधिक लोग गांव छोड़ रहे हैं। यह आंकड़ा ज़्यादा हो हो सकता है लड़कियों के वैवाहिक पलायन के कारण रिपोर्ट में सबसे बड़ा कारण आजीविका, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की कमी है।
बात अग़र खेती की करे तो उत्तराखंड में लगभग 70% जनसंख्या कृषि पर निर्भर है, लेकिन खेती राज्य के सकल घरेलू उत्पाद (GSDP) में केवल 10% से भी कम योगदान देती है। सिंचाई की व्यवस्था कुल कृषि भूमि का सिर्फ 12-15% हिस्से में ही है।
बाजार से जुड़ाव की कमी, मूल्य समर्थन न होना और आधुनिक कृषि तकनीकों की अनुपलब्धता ने इसे घाटे का सौदा बना दिया है।
नीतिगत सुझाव:
1. ग्राम आधारित आर्थिक मॉडल:
हर ज़िले के भौगोलिक और सांस्कृतिक अनुरूप “क्लस्टर आधारित माइक्रो इकोनॉमिक मॉडल” विकसित किया जाए जिसमें कृषि, पशुपालन, वनोपज, हस्तशिल्प, और पर्यटन को मिलाकर समेकित विकास योजना बने।
2. स्थानीय कृषि उत्पादों का ब्रांडिंग और मार्केट लिंक:
मंडुवा, झंगोरा, माल्टा, बुरांश जैसे स्थानीय उत्पादों को GI टैग दिलाकर उन्हें राष्ट्रीय और वैश्विक बाजार से जोड़ा जाए। हर जिले में “फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गनाइज़ेशन (FPO)” को तकनीकी और वित्तीय सहायता दी जाए।
3. वन नीति में स्थानीय सहभागिता:
“वन अधिकार अधिनियम 2006” को प्रभावी रूप से लागू किया जाए। “वन पंचायतों” को सशक्त किया जाए ताकि स्थानीय समुदाय वनों की देखभाल और उत्पादों के उपयोग में भागीदार बन सकें।
4. ग्राम्य युवा नीति:
गांवों में रहकर आजीविका चलाने वाले युवाओं को सरकारी नौकरियों में वरीयता, स्टार्टअप अनुदान, और सामाजिक मान्यता देने की नीति बने।
“ग्राम्य गौरव कार्ड” जैसी योजनाएं लाई जा सकती हैं, जिससे गांव में कार्यरत युवाओं को स्वास्थ्य, शिक्षा, यात्रा और ऋण सुविधा में प्राथमिकता मिले।
5. गांव आधारित शिक्षा और स्वास्थ्य का बुनियादी ढांचा:
हर 10 गांवों के लिए एक बहुउद्देश्यीय स्वास्थ्य केंद्र, और डिजिटल शिक्षा युक्त एक मॉडल स्कूल स्थापित किया जाए। इससे शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए पलायन रुकेगा।
उत्तराखंड की असल ताकत उसके गांवों में है। जब तक गाँवों को विकास की धुरी नहीं बनाया जाएगा, तब तक यह पर्वतीय प्रदेश अपनी आत्मा से कटता रहेगा।
समय आ गया है कि सरकार, समाज और नीति निर्माता मिलकर इस आत्मबोध को पुनर्जीवित करें,वरना यह राज्य केवल प्रशासनिक इकाई बनकर रह जाएगा, जिसकी आत्मा कहीं पीछे छूट चुकी होगी।